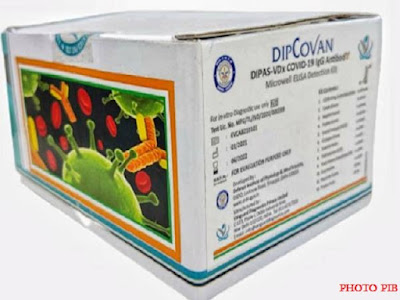अंतरिक्ष पर्यटन या वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा नई नहीं है अंतरिक्ष पर्यटन, मनोरंजन के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा है। अंतरिक्ष पर्यटन हाल ही में दो अमेरिकी अरबपतियों, रिचर्ड ब्रोंसन और जेफ बेजोस की वजह से खबरों में रहा है, जो अपने निजी रॉकेट और विमान का उपयोग करके पर्यटकों के रूप में अंतरिक्ष में गए थे।
नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई ने एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई शाखा के सहयोग से 27 जुलाई, 2021 को 'स्पेस टूरिज्म: द नेक्स्ट फ्रंटियर' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। वीएम मेडिकल सेंटर, मुंबई की एयरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डॉ. पुनीता मसरानी ने व्याख्यान में वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
अंतरिक्ष पर्यटन या वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा नई नहीं है और इसके विचार की अवधारणा से वास्तविकता तक के इतिहास पर डॉ. पुनीता ने ऑनलाइन व्याख्यान में चर्चा की। अंतरिक्ष पर्यटन, मनोरंजन के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा है। डॉ. पुनीता ने बताया कि अंतरिक्ष पर्यटन हाल ही में दो अमेरिकी अरबपतियों, रिचर्ड ब्रोंसन और जेफ बेजोस की वजह से खबरों में रहा है, जो अपने निजी रॉकेट और विमान का उपयोग करके पर्यटकों के रूप में अंतरिक्ष में गए थे।
व्याख्यान में डॉ. पुनीता ने कहा कि पहले नासा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए ले जाना शुरू किया था। यह प्रक्रिया अत्यधिक कड़ी थी। रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान हर 6 महीने में पर्यटकों को ले जाता था। 'स्पेस एडवेंचर्स अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में पहली एजेंसी थी। डॉ. पुनीता ने बताया कि एजेंसी की शुरुआत 1998 में अमेरिकी अरबपति रिचर्ड गैरियट ने की थी। एजेंसी ने रूसी सोयुज रॉकेट्स पर मध्यस्थता की सवारी की पेशकश की थी।
डॉ. पुनीता ने कहा, जबकि नासा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी दोनों ने अंतरिक्ष पर्यटन को रोक दिया, उद्योगपतियों और उद्यमियों ने सोचा कि वे निजी मिशन शुरू कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर सकें। इसने अंतरिक्ष पर्यटन की अवधारणा को जन्म दिया।
डॉ. पुनीता ने अपने व्याख्यान में कहा कि डेनिस टीटो पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री थे, जिसके पहले केवल अंतरिक्ष यात्री ही अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में जाते थे। टीटो अप्रैल 2001 में रूसी सोयुज टीएमए लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष में गए। मार्क शटलवर्थ, ग्रेग ऑलसेन, अनुश अंसारी, चार्ल्स सिमोनी, रिचर्ड गैरियट, गाइ लालिबर्टे अन्य अंतरिक्ष यात्री थे जो 2002 से 2009 के बीच अंतरिक्ष की शुल्क के साथ अंतरिक्ष यात्राओं पर गए थे। निजी अंतरिक्ष यात्रियों को कड़े चयन मानकों, व्यापक प्रशिक्षण और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपनाए गए उपायों से गुजरना पड़ता था।
डॉ. पुनीता ने निजी अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न कंपनियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की:
ब्लू ओरिजिन की स्थापना 2000 में एमज़ॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ जेफ बेजोस ने की थी। ब्लू ओरिजिन के दोबारा उपयोग होने वाले रॉकेट न्यू शेपर्ड ने हाल ही में चार निजी नागरिकों के साथ पहली मानव उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। चालक दल में जेफ बेजोस, मार्क बेजोस, वैली फंक और ओलिवर डेमन शामिल थे। रॉकेट न्यू शेफर्ड ने 20 जुलाई, 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट टेक्सास से उड़ान भरी।
स्पेसएक्स एक अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता है, जिसकी स्थापना 2002 में टेस्ला मोटर्स के एलॉन मस्क ने की थी। कंपनी ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट विकसित किया है जिसका उपयोग नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए किया था। स्पेस एक्स नागरिकों को 10 दिन की शुल्क के साथ यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने की योजना बना रहा है। स्पेस एक्स चंद्रमा और मंगल की यात्रा की भी योजना बना रहा है।
वर्जिन गेलेक्टिक की स्थापना 2004 में ब्रिटिश उद्यमी रिचर्ड ब्रैनसन ने की थी। रिचर्ड ब्रैनसन और उनका दल हाल ही में अपने वर्जिन गेलेक्टिक रॉकेट विमान पर सवार होकर न्यू मैक्सिको रेगिस्तान से 50 मील से अधिक ऊपर पहुंचे और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आए।
डॉ. पुनीता ने बताया कि जहां ये सभी मिशन अंतरिक्ष की सवारी की पेशकश करते हैं, वहीं नासा ने हाल ही में निजी नागरिकों को एक छोटी यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने की अनुमति दी है। एक्सिऑम स्पेस जैसी कंपनियां निजी अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में शामिल हैं। कंपनी भविष्य में निजी स्पेस स्टेशन की भी योजना बना रही है।
व्याख्यान में, डॉ. पुनीता ने अंतरिक्ष पर्यटन में शामिल बुनियादी शब्दावली जैसे कक्षीय उड़ानें, उप कक्षीय उड़ानें, पृथ्वी की निचली कक्षाओं के बारे में भी बताया। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के अनुसार समुद्र तल से 100 किलोमीटर से अधिक की ऊँचाई पर अर्थात् कर्मन रेखा अंतरिक्ष है। वही एजेंसी 50 मील (80.47 किलोमीटर) की ऊंचाई को अंतरिक्ष उड़ान के रूप में अर्हता प्राप्त करने की ऊंचाई मानती है।
डॉ. पुनीता ने यह भी बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट (थर्मोस्फीयर) में मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। स्टेशन 1998 में स्थापित किया गया था। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें हिस्सा लेने वाली पांच अंतरिक्ष एजेंसियां नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), जेएक्सए (जापान), ईएसए (यूरोप), और सीएसए (कनाडा)शामिल हैं।
डॉ. पुनीता ने शामिल विज्ञान और जोखिम, जागरूकता, चिंताओं और चिकित्सा सूचित सहमति पर चर्चा की जो पर्यटन का अनिवार्य हिस्सा हैं। उन्होंने आगे बताया कि उड़ान के बाद की चिकित्सा समस्याएं या स्थितियां क्या हो सकती हैं और मानव शरीर और मस्तिष्क पर अंतरिक्ष यात्रा का प्रभाव क्या हो सकता है।
नेहरू विज्ञान केंद्र के बारे में
नेहरू विज्ञान केंद्र (एनएससी) भारत के सबसे बड़े विज्ञान केंद्रों में से एक है और देश के पश्चिमी क्षेत्र में छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय है और पश्चिमी क्षेत्र में पांच अन्य विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों का संचालन और समन्वय करता है: रमन विज्ञान केंद्र, नागपुर, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, भोपाल, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, कालीकट, गोवा विज्ञान केंद्र, पणजी और जिला विज्ञान केंद्र, धरमपुर। एनएससी में एक वर्ष में 7.5 लाख से अधिक आगंतुक आते हैं। यह केंद्र स्कूली छात्रों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र और विज्ञान की समझ बढ़ाने और देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने में उत्कृष्टता का केंद्र साबित हुआ है।
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बारे में
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहाय परिषद, भारत में विज्ञान केंद्रों और विज्ञान संग्रहालयों का शीर्ष निकाय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक संगठन के रूप में कार्य करता है। यह देश भर में 25 विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय करता है। परिषद विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों, अत्याधुनिक इंटरैक्टिव प्रदर्शनों और कार्यक्रमों और विज्ञान संचार में मानव संसाधन विकास के विकास में माहिर है। परिषद को मॉरीशस के लिए टर्नकी आधार पर एक विज्ञान केंद्र विकसित करने का गौरव प्राप्त है। यह स्कूली छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता है। आईएओ के अलावा, परिषद को राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी, राष्ट्रीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता और विज्ञान एक्सपो आदि जैसे आयोजनों के लिए भी जाना जाता है। परिषद लगभग 10 मिलियन आगंतुकों और 22 ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए यात्रा संग्रहालय बसों द्वारा सेवा करती है, जिसमें विभिन्न विज्ञान केंद्रों में अपनी इंटरैक्टिव दीर्घाओं के माध्यम से 25 प्रतिशत छात्र शामिल हैं। (S0urce PIB)